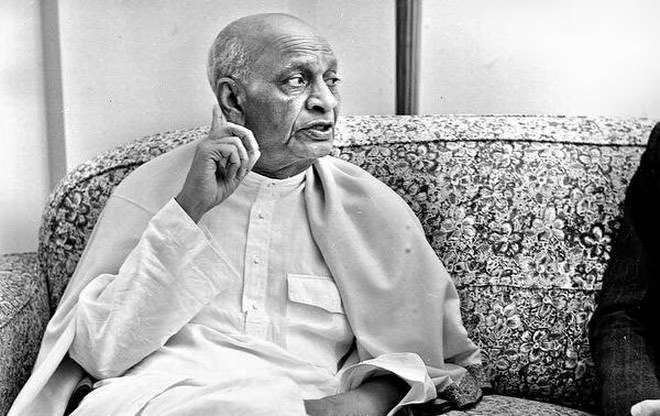भारत में बेरोज़गारी आज के समय की सबसे गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्याओं में से एक है। यह समस्या न केवल आर्थिक विकास की गति को प्रभावित करती है, बल्कि समाज की स्थिरता, युवाओं के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। बेरोज़गारी का अर्थ केवल नौकरी का न मिलना नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की विफलता भी है, जो देश के कार्यशील जनसंख्या को उपयोग में नहीं ला पा रही। एक ओर भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, तो दूसरी ओर यही युवा वर्ग रोजगार के अवसरों की कमी से सबसे अधिक प्रभावित है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बेरोज़गारी दर लगभग 5.1% के आसपास है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 4.5% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 6.5% तक पहुँच जाती है। युवा वर्ग, विशेष रूप से 15 से 29 वर्ष के बीच के युवाओं में बेरोज़गारी दर लगभग 13.8% है, जिसमें महिलाओं की दर पुरुषों से थोड़ी अधिक है। महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 14.4% है जबकि पुरुषों के लिए 13.6%। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बेरोज़गारी अब भी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है, विशेषकर तब जब देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था।
भारत में बेरोज़गारी के पीछे अनेक कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। देश की कार्यशील आयु वाली आबादी हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रम बाजार में प्रवेश कर रही है, जबकि इतने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर नहीं बन रहे। इस स्थिति ने प्रतिस्पर्धा को इतना तीव्र बना दिया है कि योग्य लोग भी नौकरी पाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण शिक्षा और कौशल में असंतुलन है। हमारे शिक्षा संस्थान अभी भी ऐसे पाठ्यक्रम चला रहे हैं जो औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं। विद्यार्थी डिग्री तो प्राप्त कर लेते हैं, पर उनके पास वह व्यावहारिक ज्ञान या तकनीकी दक्षता नहीं होती जिसकी मांग आधुनिक उद्योगों में है। यही कारण है कि स्नातक और परास्नातक युवाओं में बेरोज़गारी दर अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है।
कृषि क्षेत्र में रोजगार का स्वरूप भी इस समस्या को बढ़ाता है। भारत की बड़ी आबादी अब भी कृषि पर निर्भर है, जो मौसमी और अस्थिर व्यवसाय है। फसल के बाद के महीनों में लाखों किसान और मजदूर बेरोज़गार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितता ने कृषि को और भी असुरक्षित बना दिया है। उद्योग और सेवा क्षेत्र भी उतनी तेजी से विस्तार नहीं कर पा रहे जितनी आवश्यकता है। विनिर्माण क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने से नए रोजगार सृजन की गति धीमी पड़ी है।
तकनीकी प्रगति और ऑटोमेशन का प्रभाव भी इस संकट को गहरा कर रहा है। जहाँ मशीनें, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारंपरिक नौकरियों की जगह ले रही हैं, वहीं नयी पीढ़ी के पास उन तकनीकी कौशलों की कमी है जिनसे वे इन बदलते हालातों में खुद को ढाल सकें। यह “तकनीकी बेरोज़गारी” का नया रूप है, जो न केवल श्रमिक वर्ग बल्कि शिक्षित युवाओं को भी प्रभावित कर रहा है।
महिलाओं के रोजगार की स्थिति भी चिंता का विषय है। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएँ लगातार आगे बढ़ रही हैं, फिर भी उनकी श्रम भागीदारी दर अब भी बहुत कम है। सामाजिक मानदंड, असुरक्षित कार्यस्थल और घरेलू जिम्मेदारियाँ उन्हें कार्यक्षेत्र से दूर रखती हैं। अप्रैल 2025 में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर मात्र 26% थी, जबकि पुरुषों की लगभग 58%। यह अंतर न केवल लैंगिक असमानता को दर्शाता है, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादकता के ह्रास का संकेत भी है।
बेरोज़गारी के दुष्परिणाम बहुआयामी हैं। यह केवल आर्थिक हानि नहीं, बल्कि सामाजिक अस्थिरता का भी कारण है। जब युवा वर्ग रोजगार से वंचित रह जाता है, तो उसमें असंतोष, निराशा और हताशा जन्म लेती है। यह मानसिक तनाव, आत्महत्या और अपराध दर में वृद्धि का कारण बनता है। बेरोज़गारी सामाजिक असमानताओं को और गहरा करती है क्योंकि जिनके पास पूँजी और अवसर होते हैं, वे लाभान्वित होते रहते हैं, जबकि गरीब और पिछड़े वर्ग और अधिक हाशिये पर चले जाते हैं। पलायन, पारिवारिक विघटन और सामाजिक अशांति जैसी समस्याएँ इसी का परिणाम हैं।
इन जटिल परिस्थितियों से निपटने के लिए बहुस्तरीय और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। सबसे पहले शिक्षा और कौशल विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करना होगा ताकि युवा बदलते रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने आप को तैयार कर सकें। सरकार की “स्किल इंडिया” जैसी योजनाएँ इस दिशा में कारगर हो सकती हैं, यदि इन्हें ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए।
दूसरा महत्वपूर्ण कदम है—स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहना संभव नहीं। यदि युवाओं को स्टार्टअप्स, लघु और कुटीर उद्योगों में प्रोत्साहन दिया जाए, तो वे स्वयं के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार सृजित कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग, जैसे हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-आधारित उद्यम, बड़ी संभावनाएँ रखते हैं।
कृषि क्षेत्र में सुधार भी अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाएँ, फसल विविधीकरण और कृषि आधारित उद्योगों का विकास करके इस क्षेत्र को स्थायी रोजगार का स्रोत बनाया जा सकता है। साथ ही, औद्योगिक विकास को भी रोजगार-केंद्रित दृष्टिकोण से प्रोत्साहित करना होगा। विदेशी निवेश, विनिर्माण हब और नई औद्योगिक नीतियाँ तभी सार्थक होंगी जब वे रोजगार सृजन की दिशा में ठोस परिणाम दें।
सरकारी रोजगार योजनाओं जैसे मनरेगा को भी और अधिक प्रभावी बनाना होगा। ग्रामीण इलाकों में यह योजना करोड़ों लोगों के लिए जीवनरेखा साबित हुई है, लेकिन इसमें पारदर्शिता और स्थायित्व का अभाव अब भी चुनौती बना हुआ है। तकनीकी बदलाव के साथ तालमेल बैठाने के लिए “री-स्किलिंग” और “अप-स्किलिंग” कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ताकि जो रोजगार ऑटोमेशन के कारण खत्म हो रहे हैं, उनके स्थान पर नए अवसर तैयार किए जा सकें।
महिला रोजगार सशक्तिकरण इस पूरी प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। महिलाओं के लिए सुरक्षित और लचीले कार्यस्थल, समान वेतन और मातृत्व सुरक्षा जैसी नीतियाँ अनिवार्य हैं। जब महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होंगी, तब न केवल उनके परिवार बल्कि पूरा समाज प्रगति करेगा।
भारत में बेरोज़गारी की समस्या जटिल जरूर है, पर इसका समाधान असंभव नहीं। आवश्यकता है एक समग्र दृष्टिकोण की, जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षा संस्थान और समाज सभी की सक्रिय भागीदारी हो। जब युवाओं को कौशल, अवसर और विश्वास मिलेगा, तब वे न केवल अपनी दिशा पाएँगे बल्कि देश को भी नई ऊँचाइयों तक ले जाएँगे। रोजगार केवल आय का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय का आधार है। यदि भारत इस चुनौती को सामूहिक प्रयासों से सुलझा लेता है, तो वह न केवल आर्थिक रूप से सशक्त, बल्कि मानवीय दृष्टि से भी समृद्ध राष्ट्र बन सकता है।
– महेन्द्र तिवारी