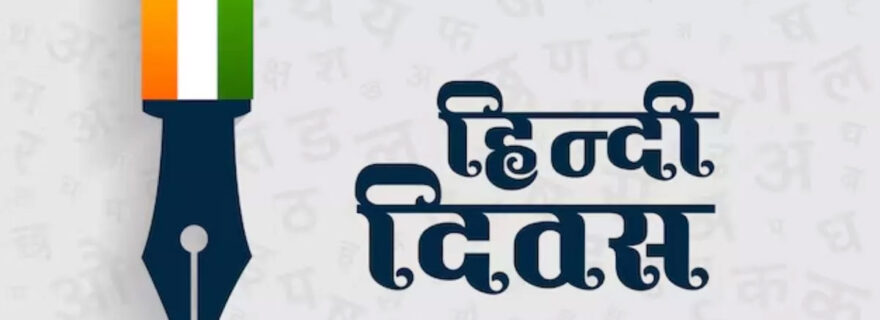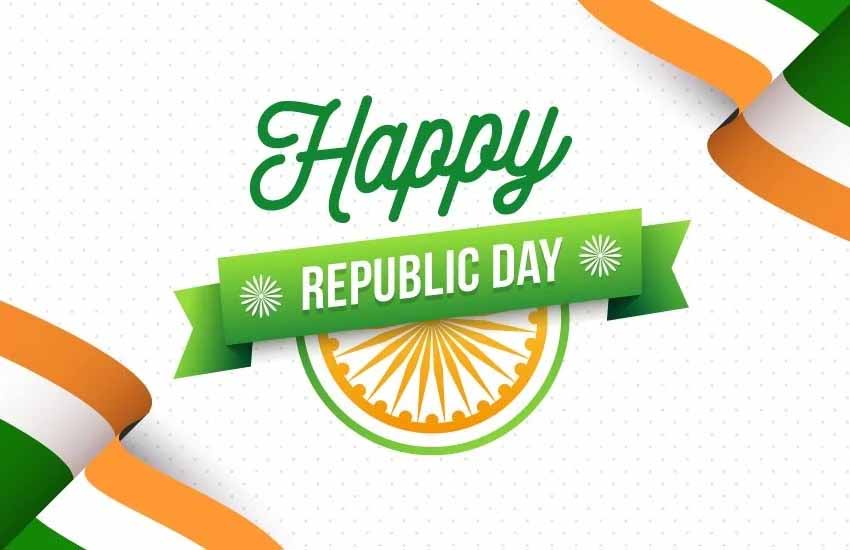भारत एक बहुभाषा-भाषी राष्ट्र है। यदि हम भारत के भाषिक अतीत पर दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि भारत में दो परिवारों की भाषाएँ बोली जाती है-आर्य-भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार, किन्तु परवर्ती युगों में जन-भाषाओं का विकास होता गया और शिष्ट या मानक भाषा के रूप-स्वरूप के स्थान पर प्रवाहमयी लोकभाषा राष्ट्रभाषा के गौरव को प्राप्त करती गयी। इतिहास साक्षी है कि राष्ट्रभाषा का गौरव सदैव मध्यदेश की भाषा को मिलता आया है। मध्यदेश राष्ट्ररूपी शरीर का हृदय है और भाषा उसका स्पन्दन। जब सारस्वत प्रदेश में द्रविड संस्कृत, अशोक काल में पाली, मध्ययुग में ब्रजभाषा और वर्तमान काल में खड़ी बोली को यह दर्जा मिला है। वस्तुतः किसी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता बल्कि समाज स्वयं इसको ग्राह्य एवं स्वीकार्य कर लेता है।
हिंदी किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह सारे राष्ट्र का प्रतीक है। सन् 1807 में टामस रोबक ने अपने शिक्षा गुरुजन गिलक्रिस्ट को लिखा था कि ‘मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या आसाम से सिन्धु के मुहाने तक इस विश्वास से यात्रा की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जायेंगे, जो हिन्दुस्तानी बोल लेते होंगे।’ इसी आधार पर राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता के लिए प्रश्रय दिया। लोकमान्य तिलक और एन०सी० केल्कर ऐनीबेसेंट ने तो यहाँ तक कहा ‘भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।’ कालान्तर में जब स्वाधीनता संग्राम की बागडोर महात्मा गाँधी के नेतृत्व में आयी तो उन्होंने यह कहकर कि ‘मेरे लिये हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है।’ राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी भाषा की अनिवार्यता सिद्ध की। इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को विकसित किया। सन् 1918 में कलकत्ता कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष के रूप में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने हिंदी में अपना भाषण पढ़ते हुए कहा कि हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यह है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी से लिया जायेगा। यह केवल गाँधी या नेताजी का स्वर नहीं था वरन् स्वामी दयानन्द, अरविन्द, सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वर भी था। सन् 1929 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा था, ‘हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, आगे चलकर यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी।’
आज भी साहित्य के क्षेत्र हिंदी ही एक मात्र भाषा है, जिसमें प्रत्येक प्रान्त के रचनाकारों की रचनाएँ मिल जाती हैं। बंगाल के क्षितिमोहन सेन, मन्मथनाथ गुप्त, महाराष्ट्र के अंततः गोपाल शेवडे, प्रभाकर माचवे तथा मुक्तिबोध, गुजरात के कन्हैया लाल मुंशी, तमिल के श्री निवासाचारी शंकर राजू, आन्ध्र के बालकृष्णराव, आरिंगपदि, केरल के चन्द्रहासन, पंजाब के यशपाल, उपेन्द्रनाथ ‘अश्क’ आदि हिंदी की राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। आज भावात्मक एकता का प्रश्न राष्ट्र का अहम प्रश्न हो गया है। हमारी संस्कृति आन्तरिक टूटन का शिकार हो रही है। अनाचार, कदाचार और भ्रष्टाचार का शिकंजा कसता जा रहा है। फैशन परस्ती एवं यांत्रिक जटिलता ने समाज को जर्जर बना दिया है। साक्षरता के प्रतिशत में वृद्धि के बावजूद शिक्षितों का अभाव हो गया है, कुलीनता का ढंग खोखला हो गया है, राष्ट्रीय अस्मिता वन्दनीय है। ऐसी स्थिति में वे स्रोत अनुसंधानित होने चाहिए जिनसे आत्म गौरव, आस्था एवं राष्ट्र के प्रति अनन्य निष्ठा का विकास हो, सांस्कृतिक संचेतना अक्षुण्ण रहे और हमारी अखण्डता अबाधित रहे।
भारत की भावात्मक एकता के खण्डित होने के पीछे कारण यह नहीं है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्थायें शक्तिहीन है, भारतीय एकता इसलिए खण्डित नहीं हो रही है कि राष्ट्रीय चेतना में अनेक संस्कृतियों का संगठन हुआ है। भावात्मक एकता को जाति, सम्प्रदाय अथवा वर्णव्यवस्था भी बाधित नहीं कर सकती है। भारतीय भावात्मक एकता में शैथिल्य इसलिए है कि हमारा जुड़ाव, हमारी संवेदनशीलता, हमारे आदान-प्रदान की माध्यम विदेशी भाषा से है। यहाँ हिंदी या उर्दू या किसी प्रान्तीय भाषा के प्रति द्वेष का भाव नहीं है। ये सारी भाषायें पहले भी थीं, उनका साहित्य पहले भी था और रहेगा। मूल बात यह है कि हमारी एकता के संयोजन सूत्र शिथिल हो रहे हैं। यदि सारे राष्ट्र की भाषा के रूप में किसी एक माध्यम को स्वीकार किया जाये तो हमारी भावात्मकता प्रबल वेग से प्रवहणशील होगी और दृढ़ता के साथ कहा जा सकता है कि यह भाषा जन-जन में पयस्विनी की भाँति प्रवाहित हिंदी हो सकती है। जिस प्रकार गंगा-यमुना के संगम में अन्तःसलिला सरस्वती की महत्ता है उसी प्रकार उत्तर और दक्षिण के दो पाटों के बीच हिंदी की गतिशीलता होनी चाहिए। हिंदी का विरोध करने वाले यह भूल जाते हैं कि विश्व फलक पर आज भारतीय संस्कृति के प्रति जो लगाव और आकर्षण दिखायी पडता है उसकी संवाहिका यही भाषा रही है। विदेशियों का असीम अनुराग हमारी तकनीकी, वैज्ञानिक एवं राजनीतिक चिन्तन के प्रति नहीं अपितु उदात्त सांस्कृतिक विरासत दर्शन, शान्ति एवं करुणा के अजस्त्र प्रवाह के प्रति है। सुकरात से लेकर अद्यावधि पाश्चात्य संस्कृति भारतीयता की इसी सुगन्धि से सुवासित होना चाहती है। भारतीय अंग्रेजों को यह बात भले ही कटु लगे किन्तु इसमें कोई संकोच नहीं कि बोतल के दूध को पीकर माँ के दूध को लजाने वाला कभी निर्भीक, मेधावी और मनीषी नहीं बन सकता। हिंदी हमारी माँ है, वह शक्ति है, ऊर्जा है, हमारी गति है, संजीवनी है। हिंदी संतों के प्रेम और करुणा की भाषा है, उसका माधुर्य, मार्दव एवं तारल्य हमें प्राणवान बनाता है।
जिन राष्ट्रों में शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा है वहाँ शिक्षितों का प्रतिशत शत-प्रतिशत है किन्तु जहाँ शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा है वहाँ 10 प्रतिशत । इसका कारण है सर्जना एवं अभिव्यक्ति की भाषा का विलगाव। हम मनुष्य हैं, संवेदनशील हैं। संवेदना का सम्बन्ध आत्मा से होता है और आत्मिक एकता का सूत्र अभिव्यक्ति के साधनों से जुड़ा है। अभिव्यक्ति का माध्यम बदल गया है। यह मानते हुये भी कि हमारा समग्र देश हिंदी भाषा को समझता है, विद्वता के आवरण में कुछ विद्वान विदेशी भाषा के मोहताज होते हैं और विदेशों में जाने पर ऐसे नकली विद्वानों की घिग्घी बंध जाती है। आँकड़ों से स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी भाषा में 33 प्रतिशत प्राप्त करने वाला सर्वाधिक अंको से उत्तीर्ण माना गया। विदेशी भाषायें सीखी जायें, प्रान्तीय भाषायें जीवन्त हों, किन्तु वे हमारी रोजी-रोटी से न जुड़ें। ऐसा कहने को न हो कि तब हम अंग्रेजों की रोटी खाते थे, अब अंग्रेजी की। फिर स्वतंत्रता कैसी? भारत ने बहुत कुछ पचाया है, शकों, कुषाणों, हूणों, यवनों, ग्रीकों तथा मुगलों के सैकड़ों आक्रमण झेले हैं परन्तु भारतीय महोदर में समाहित होकर सब एक रस हो गये हैं किन्तु आज यही जहर बन कर निकलना चाहता है। उस विष का पान करके शिव की भाँति विषपायी बनना होगा। राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता का सबसे बड़ा दायित्व हिंदी प्रदेशों पर है। यहाँ की भाषा ही राष्ट्रीय एकता की प्रतीक रही है और इस क्षेत्र को पूरी सहिष्णुता के साथ हिंदी के विकास के पक्ष में आगे आना होगा।
-डॉ. निर्मल सुवासिया