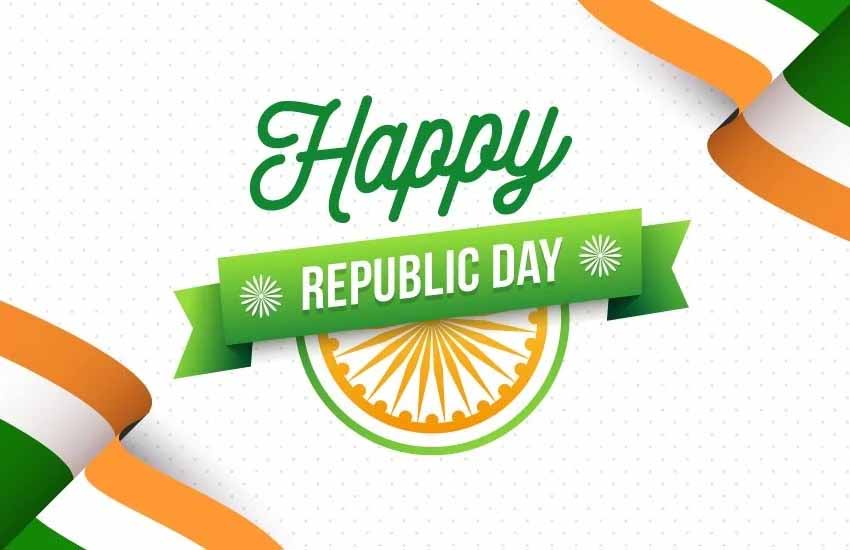हाल ही में एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक में एक खबर पढ़ी।खबर थी कि-‘पिछले 150 वर्षों में लाखों कीट प्रजातियां लुप्त हो चुकी है और हर साल शेष कीट बायोमास का 1% से 2.5% तक नष्ट हो रहा है।’ बड़ी बात यह है कि इन कीटों का पतन सिर्फ और सिर्फ महाद्वीपों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी के सबसे दूर बसे द्वीप भी इसकी चपेट में हैं।बहरहाल, यह बहुत गंभीर और चिंताजनक पर्यावरणीय मुद्दा है कि आज दुनिया भर में चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और अन्य परागण करने वाले कीट (पालीनेटर) कम हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आज दुनिया भर में कीटों का संसार खतरे में है। उल्लेखनीय है कि महाद्वीपों और द्वीपों पर कीटों के पतन को वैज्ञानिक ‘इनसेक्ट एपोकलिप्स’ यानी ‘कीट प्रलय’ के नाम से जानते हैं। वास्तव में, इनके घटने के कई कारण हैं। मसलन, इनमें क्रमशः खेती में कीटनाशकों का अंधाधुंध और अवैज्ञानिक प्रयोग, कीटों के प्राकृतिक आवासों (हेबिटेट) का लगातार नष्ट होना, जलवायु परिवर्तन, बढ़ता पर्यावरणीय प्रदूषण (मिट्टी,जल, वायु), बीमारियाँ और परजीवी आदि को शामिल किया जा सकता है। यहां तक कि प्रकाश और ध्वनि प्रदूषण भी कीटों की विलुप्ति का एक बड़ा कारण बनकर उभरा है।कहना ग़लत नहीं होगा कि खेतों में उपयोग किए जाने वाले रसायनों से मधुमक्खियों और तितलियों की मृत्यु हो रही है। यहां तक कि चींटियाँ भी इन जहरीले पदार्थों के संपर्क में आकर मर जाती हैं।जंगलों की लगातार व अंधाधुंध कटाई, शहरों का विस्तार(शहरीकरण), अंधाधुंध विकास कार्य और खेतों का एकल फसलीकरण (मोनोकल्चर) इनके प्राकृतिक निवास स्थान(नेचुरल हेबिटेट) को खत्म कर रहा है।तापमान में बदलाव, बारिश के पैटर्न में असंतुलन, और सूखा जैसी समस्याएँ कीटों के जीवन चक्र को प्रभावित कर रही हैं। आज वायरस और फंगल संक्रमण मधुमक्खियों और अन्य कीटों की जनसंख्या को तेजी से कम कर रहे हैं। वास्तव में कीटों को आज बचाने की, इनका संरक्षण करने की आवश्यकता है, क्यों कि ये जहां एक ओर परागण में भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी ओर कीट जैव विविधता के संतुलन को बनाए रखने के साथ ही साथ पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। पाठक जानते होंगे कि मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और अन्य कीट पौधों को परागित करते हैं। इससे फल, सब्ज़ियाँ और अनाज उत्पन्न होते हैं। इनके बिना खाद्य श्रृंखला(फूड चेन) प्रभावित हो सकती है। पाठकों को बताता चलूं कि चींटियाँ और अन्य कीट मिट्टी को समृद्ध बनाने, पोषक तत्वों के चक्र में मदद करने और अन्य जीवों के लिए भोजन का स्रोत हैं। इनके घटने से पारिस्थितिकी तंत्र(इको सिस्टम) असंतुलित(इमबेलेंस) हो सकता है, जिससे अन्य जीवों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यहां कहना ग़लत नहीं होगा कि धरती पर कीट प्रलय यानी कीटों (जैसे – मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, भृंग, चींटियाँ, मक्खियाँ आदि) की संख्या में बहुत बड़े पैमाने पर गिरावट या समाप्ति से गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं, इसलिए कीटों को बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम् है। धरती पर हर जीव,हर कीट, हर वनस्पतियां महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरण का अपना एक सिस्टम है और पर्यावरण के किसी भी घटक को नुकसान पहुंचने से पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य को हर हाल में नुकसान पहुंचेगा।कीट नहीं होंगे तो परागण संकट पैदा हो जाएगा। दरअसल, फसलों का परागण मुख्य रूप से मधुमक्खियों और तितलियों द्वारा ही होता है। इनके कम होने से फल, सब्जियाँ, बीज, और अनाज की पैदावार घटेगी। खाद्य सुरक्षा संकट उत्पन्न होगा और कीमतें बढ़ सकती हैं।कीट अनेक जीवों का भोजन हैं जैसे कि पक्षी, छिपकली, मेंढक, चमगादड़ आदि और यदि कीट नहीं होंगे तो इन जीवों के समक्ष जीवन का खतरा पैदा हो जाएगा।सच तो यह है कि कीट घटने से पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी, जिससे जैव-विविधता का नुकसान होगा।कई पौधों के प्रजनन के लिए कीट आवश्यक हैं।कीट नहीं होंगे तो वनस्पति भी कहीं न कहीं अवश्य ही प्रभावित होगी। तथ्य यह है कि इनके बिना जंगलों और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार रुक जाएगा। हमें यह बात अपने जेहन में रखनी चाहिए कि कुछ कीट रोग फैलाते हैं, लेकिन कई उपयोगी कीट रोग नियंत्रित भी करते हैं। कीट नहीं होंगे तो मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, जैसा कि संतुलन बिगड़ने से रोगों का प्रसार बढ़ सकता है। कीटों के नहीं होने से आर्थिक नुकसान पहुंचेगा और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। कहना ग़लत नहीं होगा कि किसानों की आय घटेगी, खाद्यान्न संकट बढ़ेगा और सामाजिक असमानता भी बढ़ सकती है। कीटों की आबादी कम होने से प्राकृतिक पुनर्चक्रण रुक जाएगा, जैसा कि कई कीट मृत जीवों को विघटित कर पोषक तत्वों को मिट्टी में लौटाते हैं। सच तो यह है कि इनके बिना जैविक कचरा बढ़ेगा और मिट्टी की गुणवत्ता खराब होगी। इतना ही नहीं, जलवायु और पर्यावरण पर भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेंगे। वनस्पति और पारिस्थितिकी पर असर पड़ने से कार्बन अवशोषण कम होगा। यहां तक कि जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया और तेज़ हो सकती है। बहरहाल, प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक ने यह लिखा है कि जापान के ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एन्टोमोलॉजिस्ट इवान इकोनोमो ने फिजी द्वीपसमूह की चींटी प्रजातियों के जीनोम विश्लेषण से बताया है कि यहां स्वदेशी चींटी प्रजातियां 79% घट गई हैं। गिरावट इंसानों के द्वीपों पर करीब 3,000 साल पहले आगमन के साथ शुरू हुई और पिछले 300 वर्षों में यूरोपीय संपर्क, वैश्विक व्यापार और आधुनिक कृषि के फैलाव के साथ तेज हो गई। यह शोध जर्नल साइंस में प्रकाशित हुआ है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि (वैज्ञानिकों के अनुसार), पृथ्वी पर लगभग 5.5 मिलियन कीट प्रजातियाँ हो सकती हैं, जिनमें से लगभग 1 मिलियन को ही अब तक वैज्ञानिकों ने पहचाना और नामित किया है। इसका अर्थ यह है कि लगभग 80% कीट प्रजातियाँ अभी भी अज्ञात हैं, जो जैविक अनुसंधान के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रस्तुत करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) के अनुसार, जुलाई 2016 तक 58 कीट प्रजातियाँ पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, जबकि 46 प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं और एक प्रजाति केवल वन्यजीवों में ही विलुप्त हो चुकी है। यहां यदि हम कीटों की विलुप्ति दर की बात करें तो वैश्विक स्तर पर, पिछले 150 वर्षों में कीटों की लगभग 5% से 10% प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, जो लगभग 250,000 से 500,000 प्रजातियों के बराबर है। गौरतलब है कि जर्मनी में 63 नेचर रिजर्व्स में उड़ने वाले कीट 30 वर्षों में 75% तक घट गए। इतना ही नहीं, अमरीका में बीटल की संख्या 45 वर्षों में 83% घटी और तितलियों की कई प्रजातियां संकट में हैं। यूरोप की घासभूमि में तितलियों की आबादी केवल एक दशक में 36% घटी है।कीट प्रलय का असर भारत में भी दिख रहा है।एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मेलघाट, महाराष्ट्र में प्रकाश प्रदूषण ने मेफ़्लाई और अन्य कीटों की संख्या को लगभग 2% प्रति वर्ष की दर से घटा दिया है। जंगलों के पास बने रिसॉर्ट्स और उनकी तेज रोशनी कीटों के प्राकृतिक चक्र को तोड़ रही है। भारत के हिमालय प्रदेश में मधुमक्खियों और तितलियों जैसे परागणकर्ता की संख्या और विविधता लगातार घटती चली जा रही है।पश्चिमी घाट, जिसे भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, में कीटों की संख्या में गिरावट एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। यह क्षेत्र 6,000 से अधिक कीट प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई प्रजातियाँ केवल यहीं पाई जाती हैं। एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी घाट में तापमान में लगभग 0.8°C की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कीटों की विविधता और संख्या में गिरावट का कारण बन रही है। आंकड़े बताते हैं कि पुणे जिले में आठ ड्रैगनफ्लाई प्रजातियाँ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गई हैं, जबकि 27 नई प्रजातियाँ पाई गई हैं, जो पर्यावरणीय बदलावों का संकेत देती हैं। इतना ही नहीं, पश्चिमी घाट की बात करें तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च बताती है कि सुरक्षित जंगलों में मूल चींटी प्रजातियां फल-फूल रही हैं, लेकिन कॉफी, चाय और रबर के बागानों में आक्रामक प्रजातियां हावी हो रही हैं। बहरहाल,कीटों की गिरती संख्या न केवल पारिस्थितिकी तंत्र(इको सिस्टम) के लिए, बल्कि मानव जीवन के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि ये परागण, पोषक चक्रण और खाद्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इसलिए, हमारे देश में विशेषकर पश्चिमी घाट में कीटों की विविधता और संख्या की रक्षा के लिए तत्काल और प्रभावी संरक्षण उपायों की आवश्यकता है। आज कीटों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मसलन, इसके लिए हमें यह चाहिए कि हम रसायनों (कीटनाशकों) के उपयोग में कटौती करें। आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। हमें यह चाहिए कि हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दें। कीटों के प्राकृतिक आवासों की हर हाल में रक्षा करें। वैज्ञानिक अनुसंधान और नीति निर्माण इस दिशा में सकारात्मक कदम साबित हो सकते हैं। कीटों की विलुप्ति एक गंभीर पर्यावरणीय संकट है, लेकिन यदि समय रहते जागरूकता, नीति और सामूहिक प्रयास किए जाएं, तो इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। चाहे पर्यावरण प्रेमी हों या नीति निर्माता, यह विषय सबके लिए महत्वपूर्ण है।
-सुनील कुमार महला