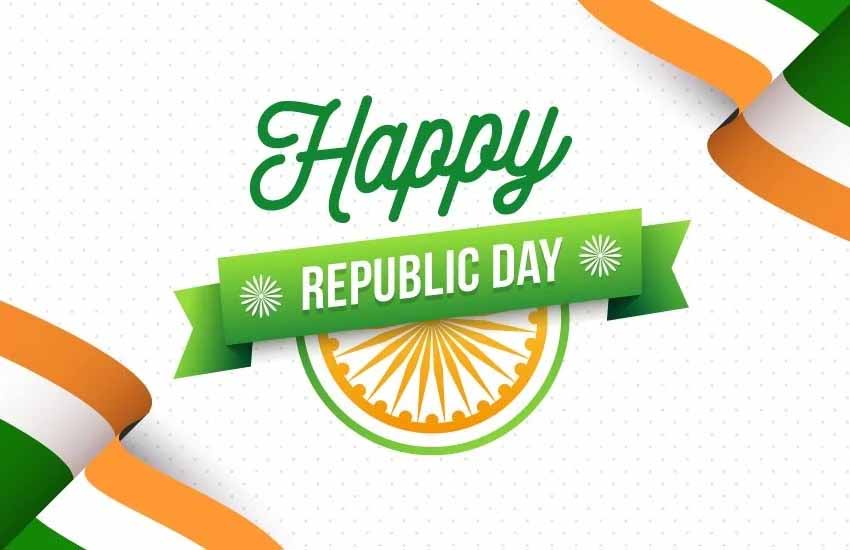ब्राजील के बेलेम में 10 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन (कॉप-30) शुक्रवार को (21 नवंबर 2025) खत्म हो गया। उम्मीद जताई गई कि बेहतर भविष्य के लिए सभी देश मिलकर काम करेंगे, लेकिन जैसी उम्मीद की जा रही थी,वैसा कुछ खास हासिल नहीं हुआ। पाठकों को बताता चलूं कि कॉप सम्मेलन(कान्फ्रेंस आफ पार्टीज) का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों को एक साझा मंच पर लाना है, जहाँ वे पर्यावरण संरक्षण, ग्रीनहाउस गैसों में कमी, तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने और टिकाऊ वैश्विक विकास की दिशा में सामूहिक निर्णय लेते हैं। जानकारी के अनुसार सम्मेलन के आखिरी दिन जीवाश्म ईंधन(कोयला , पेट्रोलियम (कच्चा तेल) और प्राकृतिक गैस) को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने को लेकर जिस तरह की खींचतान होती रही, वह दुनिया को बहुत आश्वस्त करने वाली नहीं थी। कितनी बड़ी और आश्चर्यजनक बात है कि जिस वैश्विक योजना का जिक्र कॉप सम्मेलन के शुरुआती ड्राफ्ट में था, उसे बाद के संशोधित ड्राफ्ट से हटा ही दिया गया। इससे यह साफ है कि जीवाश्म ईंधन से जुड़े विवाद जल्द सुलझने वाले नहीं हैं। यह सम्मेलन 10 नवंबर 2025 को शुरू हुआ था और उम्मीद थी कि दुनिया के तमाम देश ‘ग्लोबल वार्मिंग’ के खिलाफ कोई ठोस फैसला लेंगे, लेकिन सम्मेलन धीमी रफ्तार से आगे बढ़ा,और कुछ विशेष सामने नहीं आया। इस बार हुए कॉप-30 से उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा थीं, क्योंकि पेरिस समझौते को दस साल पूरे हो चुके हैं। यहां पाठकों को बताता चलूं कि पेरिस जलवायु समझौता वर्ष 2015 में दुनिया के लगभग सभी देशों के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ते वैश्विक तापमान को नियंत्रण में रखना है, ताकि धरती को जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों से बचाया जा सके। इस समझौते के तहत देश यह प्रयास करते हैं कि पृथ्वी का तापमान औद्योगिक युग से पहले की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे और संभव हो तो 1.5 डिग्री तक सीमित किया जाए। हर देश अपनी क्षमता के अनुसार ग्रीनहाउस गैसों में कमी लाने की योजना बनाता है, जिसे एनडीसी मतलब ‘नेशनली डेटेरमाइंड कंट्रीब्यूशन्स’ (यह वह योजना है जिसे हर देश खुद बनाता है कि वह कितनी ग्रीनहाउस गैसें कम करेगा, पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाएगा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कैसी तैयारी करेगा) कहा जाता है। साथ ही, विकसित देश गरीब और विकासशील देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं, ताकि वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा सकें। यह समझौता पूरी दुनिया को जलवायु संकट से बचाने का सामूहिक प्रयास है। बहरहाल, यहां यह कहना ग़लत नहीं होगा कि आज पूरी दुनिया जिस गंभीर जलवायु संकट से गुजर रही है, वह किसी से छिपा नहीं है। इसके बावजूद ज्यादातर देश अब भी ग्लोबल तापमान को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और 1.5 डिग्री के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति गंभीर नहीं दिखते। ऐसे में विकासशील देशों की स्थिति और भी चिंताजनक है, क्योंकि जलवायु संकट में उनका योगदान सबसे कम है, लेकिन नुकसान उन्हें सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों से बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और असहनीय गर्मी ने आज मानव जीवन को चुनौती दे दी है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि विकसित देश अपने वादों को ठीक से पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस सम्मेलन में इस बात को साफ कहा है कि विकसित देशों को तय समय से पहले ‘नेट-जीरो’ लक्ष्य हासिल करना चाहिए।उनकी यह बिल्कुल उचित मांग है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण उन्हीं देशों ने किया है, इसलिए जिम्मेदारी भी उनकी ज्यादा बनती है। यहां गौरतलब है कि विकसित देशों में प्रदूषण का स्तर उनकी ऊँची ऊर्जा-खपत और औद्योगिक गतिविधियों के कारण स्वाभाविक रूप से अधिक रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इन्हीं देशों की रही है। आंकड़े बताते हैं कि साल 1850 से 2019 तक उत्तरी अमेरिका और यूरोप ने कुल उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा पैदा किया। आज भी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में विकसित देश काफी आगे हैं; जहां उच्च-आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करीब 8–9 मीट्रिक टन तक है, वहीं विकासशील देशों में यह लगभग आधा होता है। यद्यपि तकनीक, नियमों और बेहतर निगरानी के कारण इन देशों ने वायु-गुणवत्ता में सुधार किए हैं, और कुछ देश पीएम₂.₅ प्रदूषण को विश्व स्वास्थ्य संगठन मानकों के अनुरूप रखने में सफल भी हुए हैं, फिर भी वैश्विक तापमान वृद्धि और ग्रीनहाउस गैसों की समस्या में उनका योगदान निर्णायक बना हुआ है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन की अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में विकसित देशों से अधिक जिम्मेदारी और तेज उत्सर्जन-कटौती की अपेक्षा की जाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में, भारत ने बेहतर उदाहरण पेश किया है। विकास भी जारी है और पर्यावरण संरक्षण भी। यह काबिले-तारीफ है कि साल 2005 से अब तक भारत ने अपने कार्बन उत्सर्जन में 36% से ज्यादा कमी की है, और बिजली उत्पादन में गैर-जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा 50% से अधिक हो चुका है। हाल फिलहाल,यह भी माना जा रहा है कि भारत 2070 से पहले ही नेट-जीरो का लक्ष्य हासिल कर सकता है। सम्मेलन में एनडीसी का मुद्दा भी उठा, लेकिन भारत ने भरोसा दिलाया है कि 2035 तक संशोधित एनडीसी समय पर घोषित कर दिए जाएंगे और पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट भी जारी कर दी जाएगी।अंत में,यही कहूंगा कि कॉप-30 सम्मेलन का मुख्य ध्यान तीन बातों पर केंद्रित था। मसलन, देश जलवायु कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाएँगे, जरूरतमंद देशों को तकनीक और वित्तीय मदद कैसे मिलेगी, और दुनिया मिलकर जलवायु प्रयासों को कैसे आगे ले जाएगी ? वास्तव में, अब पेरिस समझौते को लागू करने के लिए समय बहुत कम बचा है। इसलिए विकासशील देशों के हितों को प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने संकट में कम योगदान दिया है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा वही झेल रहे हैं। अब सबकी नजरें तुर्की में होने वाले कॉप-31 पर हैं, इस उम्मीद के साथ कि वहां से कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय निकल सके।
-सुनील कुमार महला