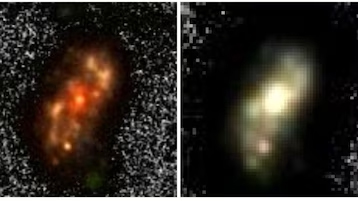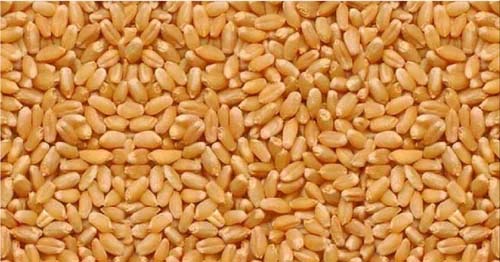डोनाल्ड ट्रंप का नाम 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के संभावित दावेदारों में शामिल जरूर था, मगर अंततः यह पुरस्कार वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के नाम हो गया। भले ही इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप से छिन गया, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा अब भी कायम है। उनके लिए यह महज एक पुरस्कार नहीं, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी ओबामा को पछाड़ने और इतिहास में अपनी जगह पक्की करने की लड़ाई है। शायद आने वाले वर्षों में यह प्रतिस्पर्धा फिर लौटे—क्योंकि ट्रंप का राजनीतिक सफर और उनका नोबेल सपना, दोनों ही कभी सुर्खियों से बाहर नहीं रहते। सवाल यह उठता है कि इतने प्रभावशाली नेता होने के बावजूद ट्रंप के हाथ यह सम्मान क्यों नहीं लगा?
नोबेल शांति पुरस्कार की प्रक्रिया सख्त और पारदर्शी है। इसे अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के आधार पर स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार हर साल उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानव जाति के लिए सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया हो। नामांकन का अधिकार किसी भी आम व्यक्ति को नहीं होता—सिर्फ अधिकृत व्यक्ति, जैसे राष्ट्राध्यक्ष, सांसद, प्रोफेसर, न्यायाधीश या पूर्व नोबेल विजेता ही किसी को नामांकित कर सकते हैं। नामांकन की अवधि हर साल सितंबर से जनवरी के अंत तक रहती है, अक्टूबर में परिणाम घोषित होते हैं और पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि, 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है।
विदेश मामलों के विशेषज्ञ डॉ. राजन कुमार के मुताबिक, ट्रंप की नाकामी के पीछे चार बड़ी वजहें थीं। पहली वजह उनके शांति प्रयासों का समय और टिकाऊपन थी। नोबेल समिति उस शांति को ज्यादा महत्व देती है, जो दीर्घकालिक हो और समय की कसौटी पर खरी उतरे। ट्रंप के हालिया प्रयास, जैसे गाजा में युद्धविराम और यूक्रेन सम्मेलन, सितंबर 2025 में हुए—जबकि नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी। यानी उनके कदम देर से उठे। समिति तब तक तय कर चुकी थी कि उस वर्ष का नोबेल किस दिशा में जाएगा। उनके समझौते अगर पहले हुए होते और उनके स्थायित्व का प्रमाण मिलता, तो शायद स्थिति कुछ अलग होती।
दूसरी वजह थी ट्रंप की वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं से दूरी। नोबेल शांति पुरस्कार का मूल उद्देश्य राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना है, जो सहयोग और सामूहिक प्रयास से ही संभव है। लेकिन ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से टकराव लिया। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की फंडिंग रोक दी, पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाला और NATO देशों पर रक्षा खर्च को लेकर दबाव बनाया। इन कदमों से अमेरिका की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा और यह धारणा बनी कि ट्रंप शांति से अधिक सत्ता और प्रभुत्व की राजनीति में रुचि रखते हैं।
तीसरी वजह थी उनका जलवायु परिवर्तन के प्रति रुख। आज के दौर में नोबेल समिति जलवायु परिवर्तन को वैश्विक शांति का दीर्घकालिक खतरा मानती है। बढ़ते तापमान, सूखे और विस्थापन जैसी समस्याएं अंततः संघर्षों को जन्म देती हैं। ऐसे में किसी भी नेता का जलवायु के प्रति दृष्टिकोण उसकी शांति की योग्यता को प्रभावित करता है। ट्रंप ने खुलेआम कहा था कि “क्लाइमेट चेंज एक धोखा है” और उन्होंने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकाल लिया था। यह कदम नोबेल समिति की दृष्टि में उन्हें ‘अयोग्य’ साबित करने के लिए काफी था।
चौथी और शायद सबसे निर्णायक वजह थी नोबेल समिति की स्वतंत्रता और उस पर ट्रंप का दबाव बनाने का प्रयास। नोबेल समिति सदैव राजनीतिक दबाव से दूर रहना चाहती है। लेकिन ट्रंप ने कथित रूप से इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पाकिस्तान सरकार से अपने नामांकन के लिए सिफारिश करवाई, और यहाँ तक कि नॉर्वे के वित्त मंत्री को फोन कर खुद के लिए नोबेल की सिफारिश की बात कही। इन सबने समिति पर गलत असर डाला। उनके इस व्यवहार ने यह संदेश दिया कि ट्रंप शांति पुरस्कार को एक “राजनीतिक ट्रॉफी” के रूप में देख रहे हैं, न कि एक नैतिक मान्यता के रूप में।
इस वर्ष नोबेल के लिए कई अन्य नाम भी चर्चा में थे। उनमें एलन मस्क का नाम था, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार माने जाते हैं। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, जो पर्यावरणीय संतुलन को शांति से जोड़ती हैं, भी मजबूत उम्मीदवार थीं। रूस में मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली यूलिया नवलनया, सूडान में मानवीय सहायता देने वाले इमरजेंसी रिस्पॉन्स रूम्स, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली संस्था ‘कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स’, दक्षिण एशिया में मध्यस्थता करने वाले अनवर इब्राहिम और गरीबों व पर्यावरण के लिए काम करने वाले पोप फ्रांसिस—इन सबका योगदान गहरा और स्थायी था। इन सबके बीच ट्रंप के प्रयास अस्थायी और आत्मकेंद्रित लगे।
लेकिन सवाल यह भी है कि ट्रंप को इस पुरस्कार को पाने की इतनी बेताबी क्यों थी? डॉ. राजन कुमार बताते हैं कि इसकी दो प्रमुख वजहें थीं। पहली, वे खुद को उन अमेरिकी राष्ट्रपतियों की कतार में देखना चाहते थे जिन्हें पहले यह सम्मान मिल चुका है—वुडरो विल्सन, थियोडोर रूजवेल्ट, जिमी कार्टर और बराक ओबामा। खासतौर पर ओबामा का नोबेल ट्रंप को हमेशा खटकता रहा है। वे इसे “अयोग्य पुरस्कार” कहते रहे हैं और किसी भी कीमत पर उनसे आगे निकलना चाहते हैं। दूसरी वजह थी एक वैश्विक “पीसमेकर” की छवि बनाना। अपनी आक्रामक और विवादास्पद नीतियों के बावजूद ट्रंप दुनिया के सामने खुद को शांति का दूत साबित करना चाहते हैं। उनके लिए नोबेल पुरस्कार इस छवि का प्रतीक है।
हालांकि 2025 में उन्हें यह सम्मान नहीं मिला, मगर विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की कोशिश यहीं खत्म नहीं होगी। उन्होंने पहले से ही 2026 के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इज़राइल और हमास के बीच जो युद्धविराम योजना उन्होंने तैयार की, उसका पहला चरण लागू हो चुका है। अगर यह पूरी तरह सफल होती है और टिकाऊ साबित होती है, तो अगली बार उनका नाम नामांकन सूची में गंभीरता से लिया जा सकता है। वे अब यह भी समझ चुके हैं कि जल्दबाज़ी में दिए गए बयान या विवादास्पद निर्णय उनकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वे इस बार संयम और रणनीति से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
– महेन्द्र तिवारी